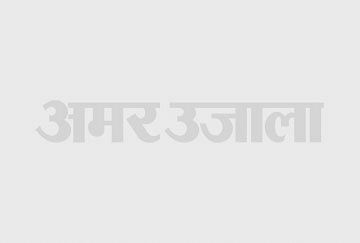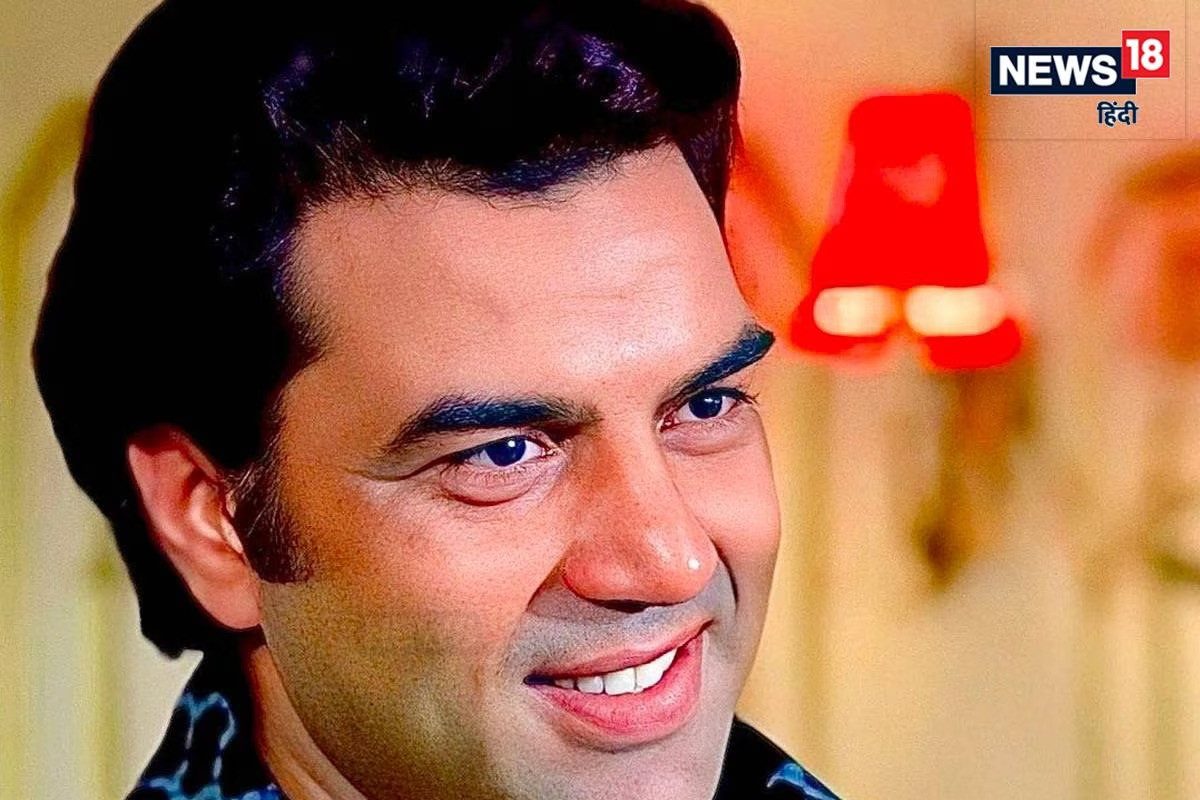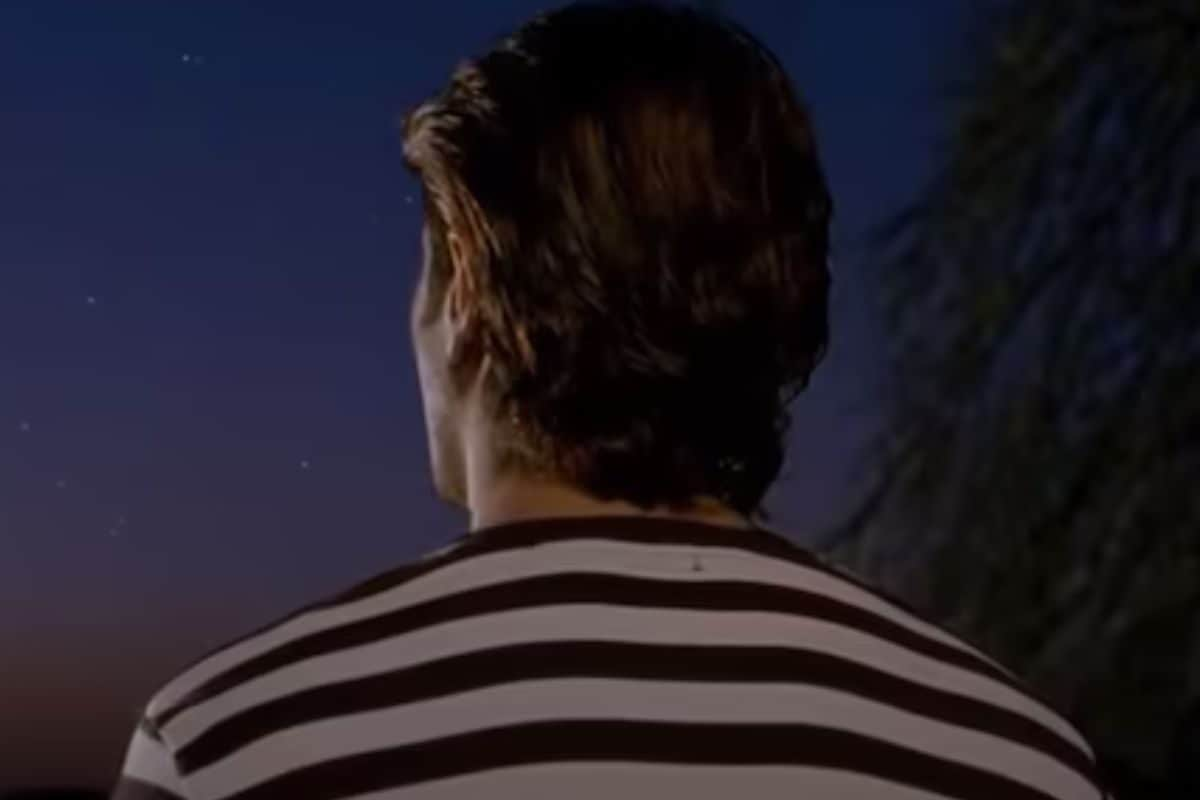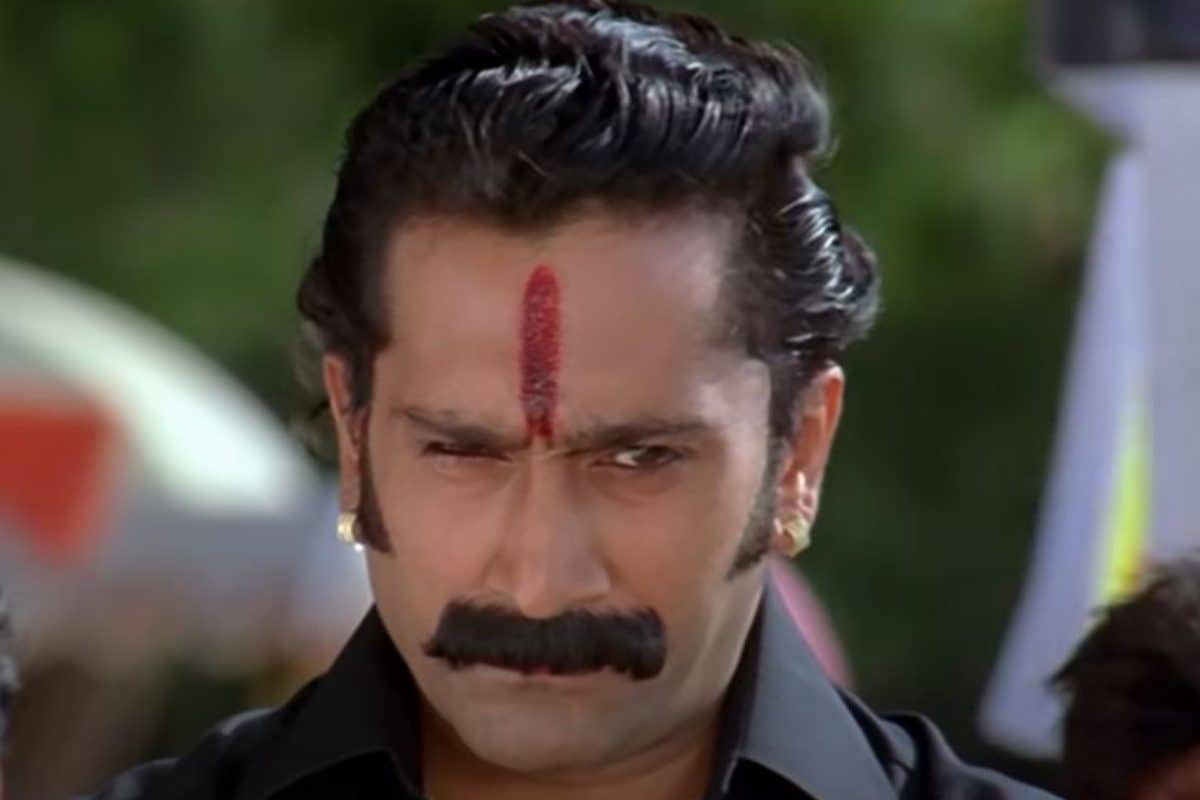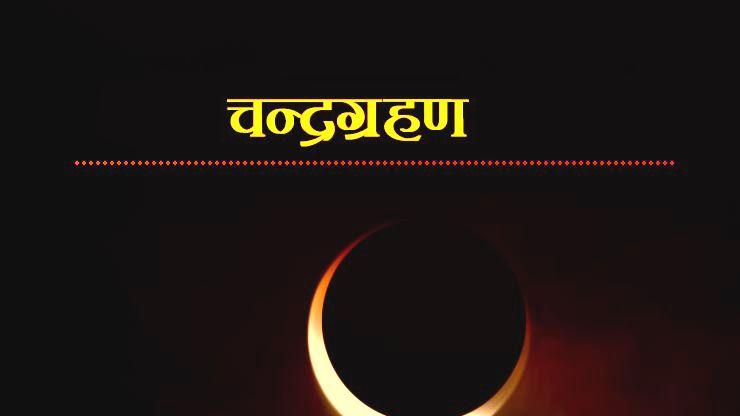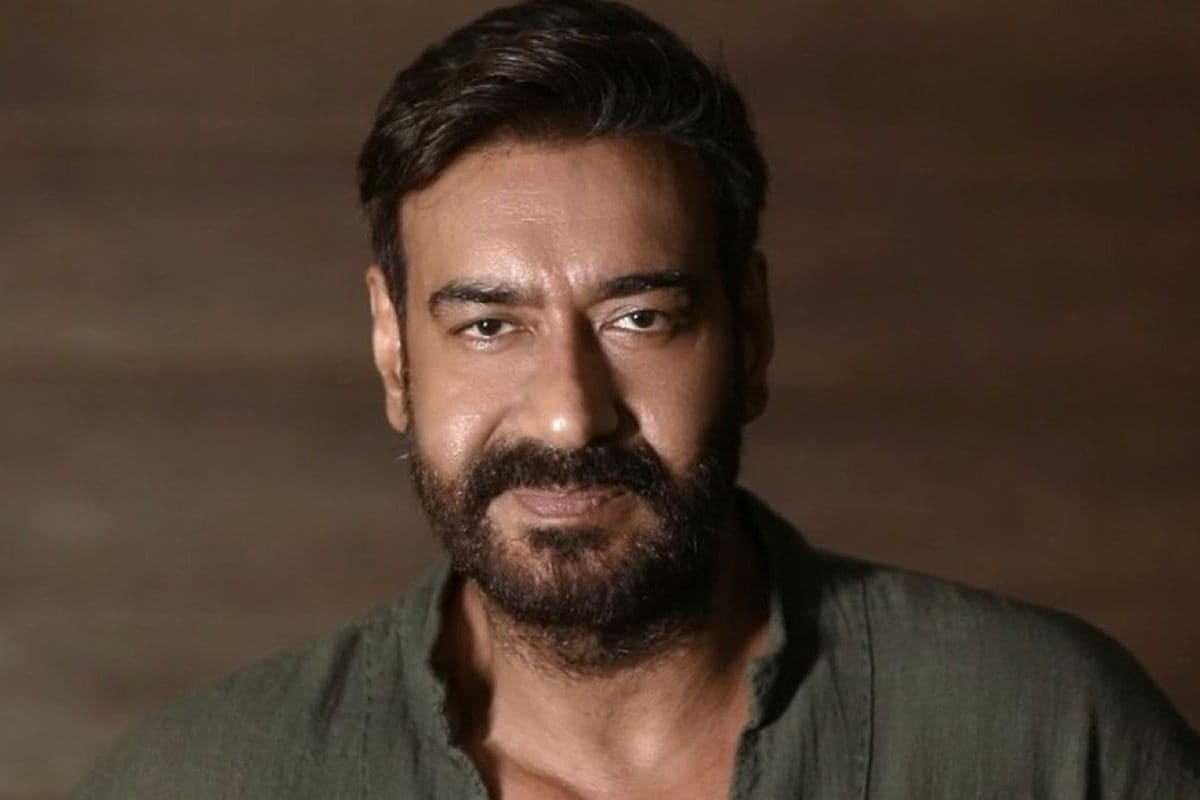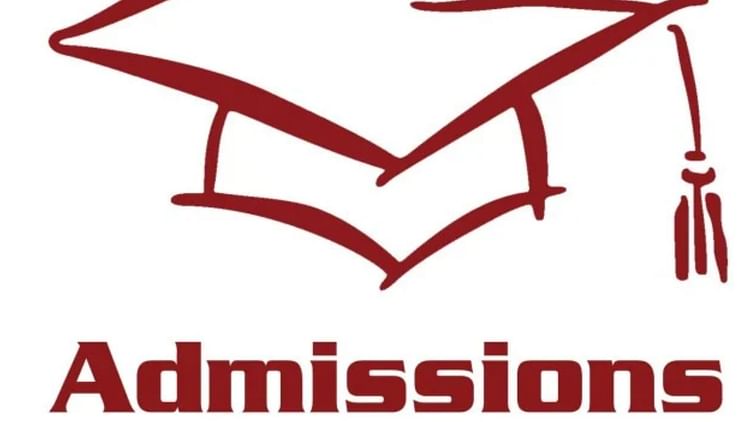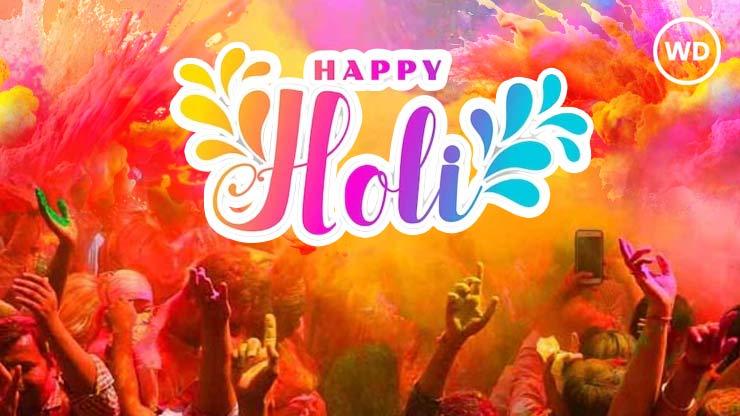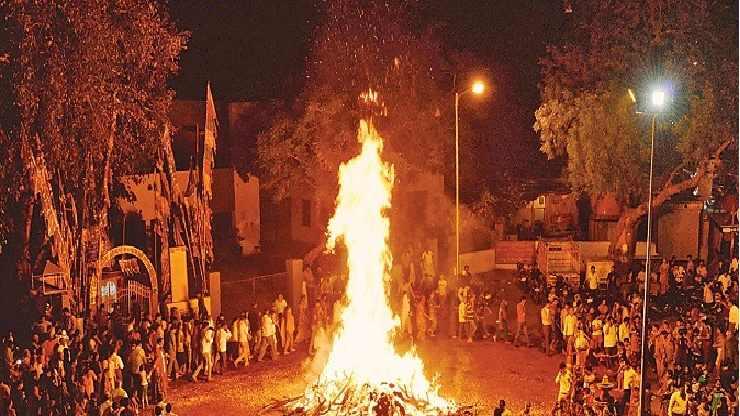निर्वाचन के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध लगातार की जा रही है कार्रवाई
admin Apr 15, 2024 0 22

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन से शुरू होगी यात्रा
admin Apr 15, 2024 0 18

एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस, भाजपा प्रत्याशी ने की थी शिकायत
admin Apr 15, 2024 0 16

जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
admin Apr 15, 2024 0 18

जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी से 24 अप्रैल तक मांगा जवाब
admin Apr 15, 2024 0 22

चैत्र नवरात्रि 2024: जानें कन्या पूजन का शुभ-मुहूर्त और पूजा विधि
admin Apr 15, 2024 0 25

राहुल गांधी के एक झटके में गरीबी खत्म वाले बयान पर पीएम मोदी का तंज, बोले- शाही जादूगर इतने समय कहां छिपा हुआ था
admin Apr 14, 2024 0 22

अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे पर बोले कैलाश विजयवर्गीय- हमारे गृहमंत्री खतरनाक आदमी, लोगों को दिन में तारे दिखा देते हैं
admin Apr 13, 2024 0 25

कमलनाथ पर कैलाश विजयवर्गीय के गंभीर आरोप, बोले- घर बुलाकर पैसा बांट रहे...
admin Apr 13, 2024 0 23